– ब्रज मोहन रामदेव
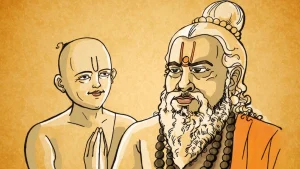
वैदिक वांग्मय के अनुसार वेद का अर्थ बोध या ज्ञान है। विद्वानों ने संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद् इन चारों के संयोग को वेद कहा है। उपनिषद् वेद का शीर्ष भाग है। अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदान्त भी कहते हैं। यह वेदों का ज्ञानवाचक भाग है। यह ज्ञान का आदिस्रोत तथा विद्या का अक्षय भण्डार है। कुल 108 उपनिषद माने जाते हैं, जिनमें दस उपनिषदों पर आदि शंकराचार्य ने अपनी टीकाएं लिखी हैं।
उपनिषद शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना तथा आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि विकसित करना है। इसके अतिरिक्त आत्म तत्व की खोज करना, चेतना को रूपान्तरित करना, मानव की अंतर्निहित क्षमताओं को जागृत करना, इन्द्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना, श्रेष्ठ मानव चरित्र का निर्माण करना आदि उपनिषद् शिक्षा के मुख्य प्रयोजन है। प्रवचन से प्रसाद (उपेक्षा) न करने का विधान व्यक्ति को शिक्षा से जीवन पर्यन्त जीवित रखता था। तैत्तिरीय उपनिषद् का उपदेश है – “स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितत्यम्।” इस अर्थ में उपनिषद् शिक्षा ऐसी प्रक्रिया थी जो जीवनभर चलती रहती थी।
उपनिषद् शिक्षा के अंतर्गत ज्ञान के दो स्वरूपों क्रमशः परा व अपरा विद्या की चर्चा की गई है। किन्तु उपनिषद् शिक्षा का मूल विषय परा विद्या है। इसलिये परा विद्या अर्थात् ब्रह्म विद्या को उपनिषद् शिक्षा में विशेष महत्व प्राप्त हैं। किन्तु अपरा विद्या को भी उपेक्षा नहीं की गई है। तैत्तिरीय उपनिषद् में गुरू अपने शिष्य से कहता है कि गृहस्थ जीवन में व्यक्तिगत सुख व समृद्धि की उपेक्षा मत करना। संतति के सूत्र को मत तोड़ना। ईशावास्योपनिवद का कथन है- “मनुष्य तु शतायु होने की इच्छा कर, लेकिन निकम्मा बैठकर नहीं, बल्कि पुरूषार्थ करता हुआ जी।” अन्न का महत्व बताते हुए उपनिषद्कार कहते हैं कि अन्न का उत्पादन बढ़ाओं, इसका संरक्षण करो। इस प्रकार हम देखते है कि उपनिषदों में परा व अपरा, दोनों प्रकार की विधाओं का उल्लेख हैं।
उपनिषदों की शिक्षण पद्धतियां
उपनिषद् शिक्षा में शिक्षण की विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया गया है, जिनमें प्रमुख निम्न हैं :
- स्व-अन्वेषण विधि : उपनिषद शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है। उपनिषदकारों की यह मान्यता रही है कि व्यक्ति ज्ञान को स्वयं के प्रयास से अन्वेषण करके प्राप्त करता है। तैत्तिरीय उपनिषद् की भृगुवल्ली में वरूण ने अपने पुत्र भृगु को इसी पद्धति से ब्रह्म का ज्ञान कराया था।
- कथा-कथन पद्धति : इस विधि में कथाओं के माध्यम से उपनिषद के गूढ़ रहस्यों को समझाया जाता था। कटोपनिषद में यम-नचिकेता की कथा, वृहदयाण्यक उपनिषद में याज्ञवलक्य मैत्रेयी संवाद, छान्दोग्य उपनिषदमें ज्ञानश्रुति और रैक्व को कथा आदि ऐसे उदाहरण है, जिन्हें कथा शैली के माध्यम से आध्यात्मिक विषयों को स्पष्ट किया गया है।
- प्रत्यक्ष अनुभव पद्धति : इस पद्धति में शिक्षार्थी को प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा ब्रह्मज्ञान कराया जाता था। छान्दोग्य उपनिषद में आचार्य आरूषि ने अपने शिष्य श्वेतकेतु को आत्मा या ब्रह्म के अस्तित्व का ज्ञान एक फल और उसके बीज को फोड़ कर देते हैं।
- कंठस्थ करने की पद्धति : इस पद्धति में वेद मंत्रों को शुद्ध उच्चारण के साथ कंठस्थ कराया जाता था। प्रारम्भ में वेदों को जब तक लिपिबद्ध नहीं किया गया था, शिष्य आचार्यों से सुनकर वेद मंत्रों को याद करते थे। आज भी कम-अधिक इस पद्धति को अपनाया जाता है।
- सूत्र प्रणाली : ज्ञान के अत्यधिक विस्तार होने के कारण उसे याद रखना कठिन हो जाता था। अतः उन्हें सूक्ष्म सूत्रों के माध्यम से स्मृति में रखा जाता था। छान्दोग्य उपनिषद् में “तत्वमसि” तथा मुण्डन उपनिषद में ‘सत्यमेव जयति नानृतं’ आदि इसी प्रकार के सूत्र कथन हैं।
- प्रतीकात्मक पद्धति : इस पद्धति में किसी वस्तु को प्रतीक मानकर शिक्षण कराया जाता था। श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है कि जिस प्रकार तिलों में तेल, दही में घी तथा अरणियों में अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा हमारी हृदय रूपी गुफा में छिपे है। जिस प्रकार अपने-अपने स्थानों में छिपा हुआ तेल, घी तथा अग्नि को उसके लिये बताए गए उपायों से उपलब्ध कराये जा सकते हैं, उसी प्रकार साधन यदि विषयों से विरक्त हो कर बताई गई विधि से तप करता है तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है।
- प्रश्नोतर विधि : शिष्य अपने आचार्य के चरणों में बैठकर आत्म ज्ञान संबंधी प्रश्न करता है तथा आचार्य उसका उत्तर योग्य विधि द्वारा देता है। प्रश्नोपनिषद उपनिषद में छः ऋषियों द्वारा महर्षि पिप्पलाद को पूछे गये प्रश्नों का उत्तर वे इसी विधि से देते हैं। उपनिषद शिक्षा में यह सबसे अधिक प्रचलित पद्धति हैं।
- स्वाध्याय विधि : तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली के नवम अनुवाक में ऋषि स्वाध्याय की अनिवार्यता बताते है। स्वाध्याय से मस्तिष्क के विकास के साथ-साथ आत्मिक उन्नति भी होती है।
- श्रवण-मनन व निदिध्यासन विधि : श्रवण, मनन व निदिध्यापन वेदांत के तीन अभ्यास है। इस विधि से व्यक्ति को पूर्ण जागृति और बोध की ओर ले जाया जाता है। इस विधि के अन्तर्गत सबसे पहले शिष्य गुरू से उपदेश सुनता है। बाद में एकाग्रचित होकर प्राप्त ज्ञान पर चिन्तन करता है। फिर बार-बार उस पर निदिध्यासन अर्थात् एकाग्र होकर ध्यान करता है। ध्यानस्थ की इस स्थिति में उसे सत्य की अनुभूति होती है। यह अनुभूति ही ब्रह्म ज्ञान की चरम स्थिति है। यह आनन्द की परम अवस्था है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि श्रवण आधारभूत ज्ञान प्रदान करता हैं । मनन अर्थात् प्राप्त ज्ञान पर चिन्तन करना है। निदिध्यासन श्रवण व मनन का परिणाम है। यह ध्यान व समाधि से प्राप्त होता है। यह ज्ञान की उच्चतम अवस्था है।
- व्याख्यान पद्धति : आचार्य द्वारा गंभीर ज्ञान को व्याख्यान एवं उपदेश द्वारा शिक्षार्थी तक पहुंचाया जाता था। व्याख्यान के पश्चात् जिज्ञासा सत्र में प्रश्नोतर विधि द्वारा शिष्य अपनी जिज्ञासा को शांत करते थे। वर्तमान में भी प्रायः इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है।
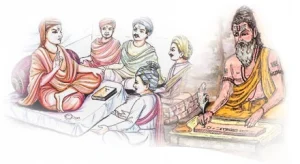
आचार्य शिष्य संबंध : उपनिषद काल में गुरू शिष्य का संबंध आत्मीय था। शिक्षार्थी अपने गुरू के कुलवासी कहलाते थे। तीव्र जिज्ञासु होना शिष्य का आवश्यक गुण माना जाता था। इसके अतिरिक्त विनय शीलता, आज्ञा पालन, मृदुभाषी और ब्रह्मचर्य का पालन करना आदि गुणों का होना भी आवश्यक माना जाता था। गुरू व शिष्य के मध्य परस्पर ज्ञान के लेन देन का संबंध है। एक ज्ञान लेता है तथा दूसरा ज्ञान देता है। दोनों मिलकर ज्ञान यज्ञ को सम्पन्न करते हैं।
पंचकोशात्मक व्यक्तित्व : तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली में पंचकोशात्मक व्यक्तित्व की संकल्पना दी गई है। यहां भृगु अपने पिता वरूण के पास ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा लेकर जाता है। भृगु अपने पिता से प्रश्न करता है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिये। पिता अपने पुत्र से कहता है कि स्वयं अनुसंधान करो और मुझे बताओ। ज्ञान प्राप्त करने की यह विद्या उपनिषद काल की अपनी विशेषता का अनुभूति से ज्ञान जितना परिपक्व होता है, उपदेश से नहीं होता। इसीलिए वरूण ने अपने पुत्र को उपदेश न देकर स्वयं साधना व अनुसंधान के लिए प्रेरित किया।
पिता की आज्ञा पर भृगु साधना को प्रवृत होता है। साधना के अनन्तर भृगु को बोध होता है कि अन्न ही ब्रह्म है। यह बात जब भृगु के पिता को बताई तो पिता ने कहा पुनः तप (अनुसंधान) करो। इस बार भृगु को बोध हुआ कि प्राण ही ब्रह्म है। पिता वरूण इस बार भी संतुष्ट नहीं हुए और पुनः साधना के लिये कहा। तीसरी बार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मन ही ब्रह्म है। पिता ने सोचा कि पुत्र इस बार कुछ गहराई तक उतरा है। उन्होंने पुत्र को पुनः गवेषणा करने का कहा। इस चौथे सोपान में भृगु ने यह निश्चय किया कि विज्ञान रूप चेतन अर्थात् जीवात्मा ही ब्रह्म है। पिता वरूण ने सोचा कि पुत्र इस बार ब्रह्म के स्वरूप के निकट पहुंचा है। उसे अभी साधना करने की जरूरत है। अतः पुत्र को पुनः तप करने का कहा। पांचवें सोपान में भृगु ने पुनः गहन चिन्तन किया। अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वास्तव में आनन्द ही ब्रह्म है। यह आनन्द मय परमात्मा ही सबकी अन्तरात्मा में विराजमान हैं। इस प्रकार भृगु को आत्मा के पांच आयामों का ज्ञान हुआ। प्रत्येक चरण में एक-एक आयाम को अनावृत करते हुए अन्त में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। अतः अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और अंत में आनन्दमय कोश की यात्रा करते हुए अन्ततः उसे ब्रह्म का ज्ञान हुआ।
व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के ये पांच आयाम हैं पंचकोशात्मक विकास ही व्यक्ति के विकास की पूर्ण संकल्पना है। सामान्य भाषा में हम इसे शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और चित कहते हैं। व्यावहारिक संदर्भ में चित को ही आत्मा मानते हैं। इस प्रकार अन्नमय कोश शरीर है, प्राणमय कोष प्राण है, मनोमय कोश मन है, विज्ञानमय कोश बुद्धि है और आनन्दमय कोश चित है। इन सभी का पूर्ण विकास पंचकोशात्मक व्यक्तित्व का विकास कहलाता है। इस पूर्ण व्यक्तित्व के दो भाग है। एक है स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर। अन्नमय कोश स्थूल शरीर है तथा प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोश मिलकर सूक्ष्म शरीर है। मृत्यु के साथ दोनों शरीर अलग हो जाते है। स्थूल शरीर अग्नि को समर्पित हो जाता है और सूक्ष्म शरीर दूसरे स्थूल से संयोग कर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। औपनिषद् शिक्षा में इसी को आधार मानकर व्यक्तित्व विकास की संकल्पना की गई हैं।
(लेखक आर्ष साहित्य के अध्येता है।)